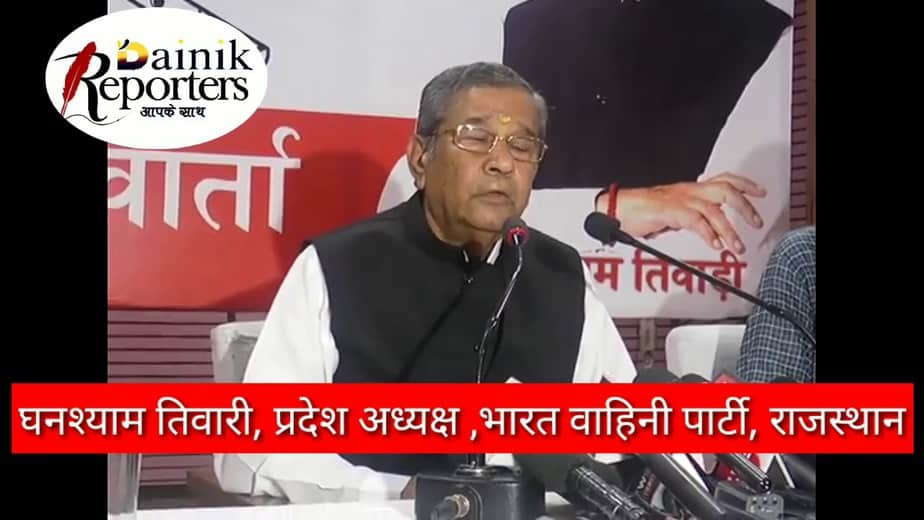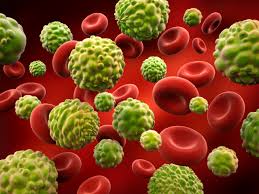असत्य ज्ञान के स्त्रोत फेसबुक और व्हॉट्सएप केंद्र के रूप में उभरे हैं
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर देश भर में फेक न्यूज ने जोर पकड़ा है। सजगता से आप भी इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पोस्ट ट्रूथ शब्द को वर्ष 2016 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। इस शब्द को एक विशेषण के तौर पर परिभाषित किया गया है, जहां निजी मान्यताओं और भावनाओं के बजाय जनमत निर्माण में निष्पक्ष तथ्यों को कम महत्व दिया जाता है। यहीं से शुरू हुआ था फेक न्यूज का सिलसिला।
फर्जी फोटो को पहचानने में गूगल और यांडेक्स ने रिवर्स इमेज सुविधा शुरू की है, जहां आप कोई भी फोटो अपलोड करके यह पता कर सकते हैं कि कोई फोटो इंटरनेट पर यदि है, तो वह सबसे पहले कब अपलोड की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशल ने वीडियो में छेड़छाड़ और उसका अपलोड इतिहास पता करने के लिए यूट्यूब के साथ मिलकर यू ट्यूब डाटा व्यूअर सेवा शुरू की है।
अनुभव यह बताता है कि 90 प्रतिशत वीडियो सही होते हैं पर उन्हें गलत संदर्भ में पेश किया जाता है। किसी भी वीडियो की जांच करने के लिए उसे ध्यान से बार-बार देखा जाना चाहिए।
लैंडलाइन फोन के युग में पूरा देश गणेश जी को दूध पिलाने निकल पड़ा था, पिछले एक दशक में सूचना क्रांति ने अफवाहों को तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से ऐसी गति दे दी है। सोशल मीडिया के तेज प्रसार और आर्थिक पक्ष ने झूठ परोसने की कला को नए स्तर पर पहुंचाया है। इस असत्य ज्ञान के स्त्रोत फेसबुक और व्हॉट्सएप केंद्र के रूप में उभरे हैं।
भारत जैसे देश में जहां लोग प्राप्त सूचना का आकलन अर्जित ज्ञान की बजाय जन श्रुतियों, मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर करते हैं, वहां भूतों से मुलाकात कर कोई भी यूट्यूब चैनल रातों-रात हजारों सब्सक्राईबर जुटा लेता है। वीडियो भले झूठे हों पर उसे हिट्स मिलेंगे तो उसे बनाने वाले को आर्थिक रूप से फायदा भी मिलेगा। विकसित देश के मुकाबले भारत में झूठ का कारोबार तेजी से गति पकडता है।
फेक न्यूज के चक्र को समझने से पहले मिसइंफोर्मेशन और डिसइंफोर्मेशन में अंतर समझना जरूरी है। मिसइंफोर्मेशन का मतलब ऐसी सूचना जो असत्य है, पर जो इसे फैला रहा है वह यह मानता है कि यह सूचना सही है। वहीं डिसइंफोर्मेशन का मतलब ऐसी सूचना से है जो असत्य है और इसे फैलाने वाला भी यह जानता है कि अमुक सूचना गलत है फिर भी वह फैला रहा है।
देश में दोनों तरह की सूचनाओं के फैलने की उर्वर जमीन मौजूद है। एक तरफ वे भोले लोग जो इंटरनेट के प्रथम उपभोक्ता बने हैं और वहां जो भी सामग्री मिल रही है वे उसकी सत्यता जाने समझे बिना उसे आगे बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ विभिन्न दलों के साइबर सेल के लोग उन झूठी सूचनाओं को इस मकसद से फैलाते हैं ताकि लोगों को संगठित किया जा सके। इन सबके पीछे खास मकसद होता है। जैसे हिट्स पाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी व्यक्ति या संस्था पर कीचड़ उछालना, साङोदारी, लाभ कमाना, राजनीतिक फायदा उठाना या दुष्प्रचार। फेक न्यूज ज्यादातर भ्रमित करने वाली सूचनाएं होती हैं या बनाई हुई सामग्री। अक्सर झूठे संदर्भ को आधार बना कर ऐसी सूचनाएं फैलाई जाती हैं।
फेक न्यूज
रिपोर्ट के अनुसार जून तक देश में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या पांच करोड़ हो चुकी थी। समस्या यहीं से शुरू होती है, भारत में लगभग 20 करोड़ लोग व्हॉट्सएप का प्रयोग करते हैं जिसमें कई संदेश, फोटो और विडियो फेक होते हैं। जागरूकता के अभाव में ये वायरल होते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के कारण व्हॉट्सएप पर कोई तस्वीर सबसे पहले किसने डाली, यह पता करना लगभग असंभव है। भारत के लिहाज से इंटरनेट एक युवा माध्यम है जिसे यहां आए 22 साल ही हुए हैं। सोशल नेटवर्किंग अभी बाल्यावस्था में ही है।
इंटरनेट पर जो कुछ है वह सच ही हो ऐसा जरूरी नहीं, इसलिए अपनी सामान्य समझ का इस्तेमाल जरूरी है।